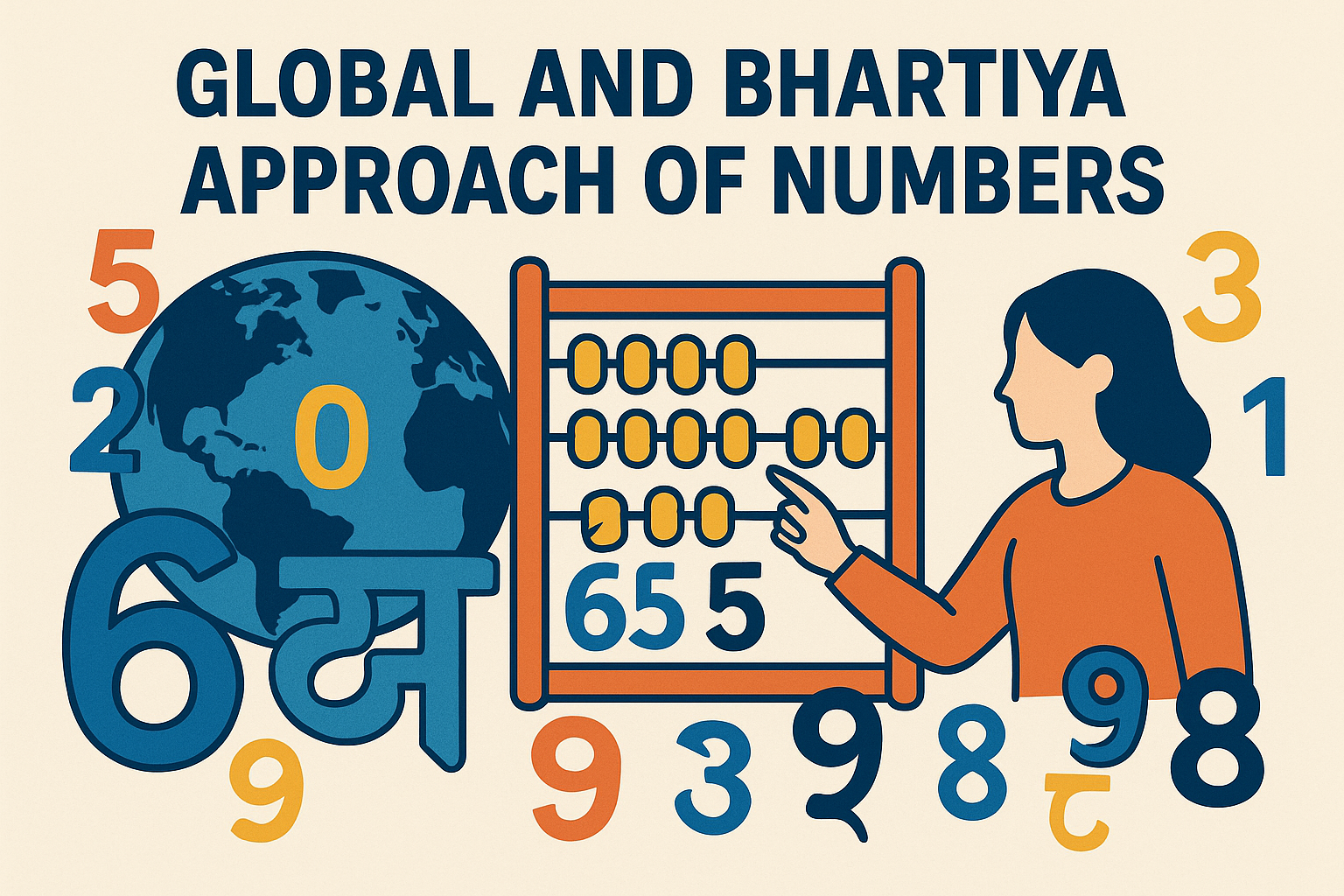अब हम वैदिक गणित में संख्या के वैश्विक और भारतीय दृष्टिकोण ( Global and Bhartiya Approach of Numbers ) की चर्चा करेंगे। संख्या को समझने के लिए कुछ अधोलिखित उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे।
जैसे धनराशि, छड़ की लंबाई, चावल की बोरी का वजन, पुरुषों की संख्या, मात्राएं हैं।(किसी राशि को इकाई राशि (या केवल इकाई) तब कहा जाता है जब उसका प्रयोग समान प्रकार की अन्य राशियों के परिमाण की तुलना करने के लिए किया जाता है।)” – (J. B. Lock)
इस प्रकार, जब हम किसी निश्चित राशि को 3 (तीन) रुपये के रूप में बोलते हैं, तो रुपये को मुद्रा की इकाई के रूप में प्रयोग किया जाता है। जब हम किसी स्कूल की किसी निश्चित कक्षा को 28 (अट्ठाईस) लड़कों वाली कक्षा के रूप में बोलते हैं, तो लड़का इकाई के रूप में प्रयोग किया जाता है।

इन्हें भी पढ़ें . . .
संस्कृत में संख्या के वैश्विक और भारतीय दृष्टिकोण ( Global and Bhartiya Approach of Numbers ) का वर्णन
महान् वैयाकरण भर्तृहरि ने अपने वाक्यपदिय ग्रंथ में कहा है –
क्रिया भेदाय कालस्तु संख्या सर्वस्य भेदिका ।
अर्थात् क्रिया काल का भेदक है परन्तु संख्या सभी द्रव्यो का उनके सभी विशेषणों का, उनकी सभी उपाधियों के विभेदीकरण का कार्य करती है।
वह जो किसी राशि के परिमाण को उसकी इकाई के सापेक्ष इंगित करता है उसे संख्या कहते हैं।
इस प्रकार, संख्या तीन, इसकी इकाई एक रुपये की तुलना में तीन रुपये की मात्रा के सापेक्ष परिमाण को इंगित करती है।
किसी मात्रा का माप या संख्यात्मक मान वह संख्या है जो यह व्यक्त करती है कि मात्रा में इकाई कितनी बार समाहित है।
इस प्रकार, यदि हम लंबाई की इकाई के रूप में एक गज का उपयोग करते हैं, और एक निश्चित लंबाई को पांच गज के रूप में बोलते हैं, तो संख्या पांच उस लंबाई का माप या संख्यात्मक मान है।
उपर्युक्त विवरण संख्या का वैश्विक और भारतीय दृष्टिकोण ( Global and Bhartiya Approach of Numbers ) को प्रदर्शित करता है ।
संख्या का स्वरुप
किसी संख्या को अमूर्त संख्या कहा जाता है, जब वह किसी विशेष इकाई से जुड़ी नहीं होती; जैसे, चार, पांच, सात।
किसी संख्या को ठोस संख्या तब कहा जाता है, जब वह किसी विशेष इकाई से जुड़ी हो; जैसे, चार घोड़े, पांच आदमी, सात गज।
अंकगणित विज्ञान का एक हिस्सा है जो संख्याओं का उपयोग सिखाता है।
संख्याओं का उपयोग गिनती, माप, लेबलिंग और गणना करने के लिए किया जाता है । वे रोजमर्रा की जिंदगी में मौलिक हैं, समय बताने और पैसे गिनने से लेकर व्यंजनों का पालन करने और माप समझने तक।
अंको के द्वारा संख्याओं को प्रस्तुत करने की विधि
अंकगणित में हम सभी संख्याओं को दस प्रतीकों या अंकों, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, जिन्हें अंक कहते हैं, के माध्यम से दर्शाते हैं। इनमें से पहले नौ अंकों को सार्थक अंक कहते हैं; अंतिम अंक को शून्य, सिफर या शून्य कहते हैं।
1 से 10: ऐतिहासिक और प्रतीकात्मक महत्व
अंक वैश्विक ऐतिहासिक महत्व
भारतीय महत्व
1 – एकता और उत्पत्ति का प्रतीक। पाइथागोरस इसे सभी संख्याओं का स्रोत मानते थे।
ब्रह्म (परम सत्य), एकता, आदि (आरंभ) का प्रतिनिधित्व करता है। संस्कृत में: एक।
2 – द्वैत: प्रकाश/अंधकार, पुरुष/स्त्री। द्विआधारी प्रणालियों का आधार।
द्वैत (द्वैत) का प्रतीक – शरीर/आत्मा, अच्छाई/बुराई, पुरुष/प्रकृति। संस्कृत में: द्वि।
3 – कई संस्कृतियों में त्रिमूर्ति (ईसाई त्रिमूर्ति, आदि)।
त्रिमूर्ति का प्रतीक – ब्रह्मा (सृष्टि), विष्णु (संरक्षण), शिव (विनाश)। साथ ही 3 गुण: सत्व, रज, तम।
4 – स्थिरता (4 दिशाएँ, 4 ऋतुएँ) का प्रतिनिधित्व करता है। चतुर्विध पुरुषार्थों – धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का प्रतीक है। वेद भी 4 हैं।
5 – पाँच उंगलियाँ, पाँच इंद्रियाँ, कई प्राचीन संस्कृतियों में महत्वपूर्ण।
पंच महाभूत – पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। पंच कर्मेन्द्रियों और ज्ञानेन्द्रियों से भी जुड़े हैं।
6 – गणित में इसे अक्सर एक पूर्ण संख्या (1+2+3=6) माना जाता है।
षड् दर्शन (भारतीय दर्शन के छह रूढ़िवादी संप्रदाय) और षण्मुख (कार्तिकेय, छह मुख वाले देवता) का प्रतिनिधित्व करता है।
7 – व्यापक रूप से पवित्र (7 दिन, 7 स्वर्ग, 7 अजूबे)।
सप्तऋषि (सात ऋषि), सप्त लोक (सात लोक), सप्त स्वर (सात स्वर)। योग में भी इसे 7 चक्र माना जाता है।
8 – अनंत का प्रतीक (क्षैतिज होने पर ∞)। पुनर्जन्म से संबद्ध। अष्ट सिद्धियों, अष्ट लक्ष्मी (धन के आठ रूप) और अष्टांग योग से संबंधित।
9 – रहस्यमय (जैसे, 3×3), एकल-अंकीय संख्याओं में अंतिम संख्या।
नवग्रह (नौ ग्रह देवता), नवरात्रि (पूजा की नौ रातें), नव दुर्गाएँ।
10 – दशमलव प्रणाली का आधार, पूर्णता, या नया चक्र। दशावतार (विष्णु के दस अवतार), दस दिशाओं (दशा दिशा) का प्रतिनिधित्व करता है। इसे पूर्णता का प्रतीक भी माना जाता है।
संख्याओं के प्रति भारतीय दृष्टिकोण (दार्शनिक + गणितीय)
1. वैदिक और दार्शनिक दृष्टिकोण:
संख्याएँ केवल मात्राएँ नहीं थीं, बल्कि उनके आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक अर्थ भी थे।
अनुष्ठानों, मंत्रों, वास्तुकला (वास्तु शास्त्र) और खगोल विज्ञान में इनका उपयोग किया जाता था।
ऋग्वेद में दार्शनिक अर्थ वाले संख्याओं के संदर्भ हैं।
2. भारत से गणितीय योगदान:
शून्य (0): भारत में आविष्कार किया गया और ब्रह्मगुप्त (7वीं शताब्दी) द्वारा औपचारिक रूप दिया गया।
दशमलव प्रणाली: स्थितीय दशमलव संख्या प्रणाली की उत्पत्ति भारत में हुई।
महान गणितज्ञ:
आर्यभट्ट: स्थान-मान प्रणाली, π का सन्निकटन।
भास्कर प्रथम और द्वितीय: बीजगणित, अंकगणित और प्रारंभिक कलन अवधारणाएँ।
पिंगला (लगभग 200 ईसा पूर्व): संस्कृत छंदशास्त्र में प्रयुक्त द्विआधारी प्रणाली।
3. अंक ज्योतिष और आयुर्वेद:
प्रत्येक अंक तत्वों, दोषों और ग्रहों से जुड़ा होता है।
ज्योतिष (वैदिक ज्योतिष) अंकों को ग्रहों के प्रभाव से जोड़ता है।
सारांश तालिका (संस्कृत नामों सहित):
संख्या प्रतीकात्मक अर्थ
1- एक, ब्रह्म, एकता, आरंभ
2- द्वि, द्वैत, संतुलन, ध्रुवता
3- त्रि, त्रिमूर्ति, गुण, सृजन, क्रिया, संहार।
4- चतुर, वेद, जीवन के लक्ष्य, आधार, पूर्णता
5- पंच, तत्व, इंद्रियाँ, भौतिक और मानसिक जगत
6- शत, दर्शन, कार्तिकेय, ज्ञान, अनुशासन
7- सप्त, ऋषि, लोक, चक्र, आध्यात्मिक विकास, पूर्णता
8- अष्ट, सिद्धियाँ, लक्ष्मी, शक्ति, प्रचुरता
9- नव, ग्रह, दुर्गा, पूर्णता, ब्रह्मांडीय क्रम
10- दशा, अवतार, दिशाएँ, पूर्णता, चक्र पूर्णता